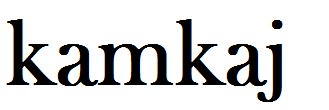भारत में उच्च न्यायालय
- किसी राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है तथा राज्य के अन्य सभी न्यायालय उसके अधीन कार्य करते हैं।
- संविधान के अनुसार, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है (अनुच्छेद 231)।
- भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
- 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय भी उसी वर्ष स्थापित किए गए थे।
- नवीनतम उच्च न्यायालय तेलंगाना न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैं, दोनों की स्थापना वर्ष 2019 में हुई।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं
- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित मद्रास लॉ जर्नल, भारत में न्यायालय के निर्णयों की रिपोर्टिंग के लिए समर्पित पहली पत्रिका थी (1891)।
भारत में कुल उच्च न्यायालय
भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है । सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष के साथ सूची नीचे दी गई है:
| भारत में उच्च न्यायालयों की सूची | |||
|---|---|---|---|
| नाम | वर्ष | प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र |
सीट |
| कोलकाता | 1862 | पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर की बेंच) |
| बंबई | 1862 | महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली। गोवा, दमन दीव | मुंबई (पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में पीठ) |
| चेन्नई | 1862 | तमिलनाडु और पांडिचेरी | चेन्नई (मदुरै में बेंच) |
| इलाहाबाद | 1866 | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद (लखनऊ बेंच) |
| कर्नाटक | 1884 | कर्नाटक | बेंगलुरू (धारवाड़ और गुलबर्गा में बेंच) |
| पटना | 1916 | बिहार | पटना |
| जम्मू और कश्मीर | 1928 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू |
| पंजाब और हरियाणा | 1947 | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| गुवाहाटी | 1948 | असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश | गुवाहाटी (कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में बेंच |
| उड़ीसा | 1948 | उड़ीसा | कटक |
| राजस्थान | 1949 | राजस्थान | जोधपुर (बेंच – जयपुर) |
| मध्य प्रदेश | 1956 | मध्य प्रदेश | जबलपुर (बेंच –इंदौर, ग्वालियर) |
| केरल | 1958 | केरल एवं लक्षद्वीप | एर्नाकुलम |
| गुजरात | 1960 | गुजरात | अहमदाबाद |
| दिल्ली | 1966 | दिल्ली | दिल्ली |
| हिमाचल प्रदेश | 1966 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| सिक्किम | 1975 | सिक्किम | गंगटोक |
| छत्तीसगढ | 2000 | छत्तीसगढ | बिलासपुर |
| उत्तराखंड | 2000 | उत्तराखंड | नैनीताल |
| झारखंड | 2000 | झारखंड | रांची |
| त्रिपुरा | 2013 | त्रिपुरा | अगरतला |
| मणिपुर | 2013 | मणिपुर | इम्फाल |
| मेघालय | 2013 | मेघालय | शिलांग |
| आंध्र प्रदेश | 2019 | आंध्र प्रदेश | अमरावती |
| तेलंगाना | 2019 | तेलंगाना | हैदराबाद |
न्यायाधीशों की नियुक्ति
किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से होती है।
न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं
वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
वह भारत के एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता अथवा भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो।
कार्यकाल:
मूलतः उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन संविधान के 15वें संशोधन के अनुसार 1963 में इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।
न्यायाधीशों को हटाया जाना
एक न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजेगा।
यदि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनका पद रिक्त माना जाएगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग बैठकर, उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने पर हटाया जा सकता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 280,000/- रुपये प्रति माह है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 250,000/- रुपये प्रति माह है।
उच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य
उच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं:
1) कुछ रिट जारी करने की शक्ति: – प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या अन्य प्रयोजन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति है।
2) अधीक्षण की शक्ति: प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।
3) मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति: यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, जिसका निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह मामले को वापस ले लेगा और-
या तो मामले का स्वयं निपटारा करें; या
उक्त विधि प्रश्न का अवधारण करेगा और मामले को उस न्यायालय को, जहां से वह मामला वापस लिया गया है, ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रति सहित वापस कर देगा और उक्त न्यायालय उस प्रति की प्राप्ति पर ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगा।
4) जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना आदि में परामर्श: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति में राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श लिया जाता है। राज्य न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति में भी उच्च न्यायालय से परामर्श लिया जाता है।
5) अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण: जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से निम्न कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति और उन्हें छुट्टी प्रदान करना शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित है।
6) अन्य मूल और अपीलीय शक्तियां: उच्च न्यायालय को सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जैसा कि सिविल और आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पेटेंट पत्रों द्वारा प्रदान किया गया है।