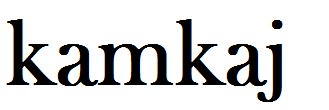भारतीय राजनीति भारत की संसद के इर्द-गिर्द घूमती है जो देश की राजधानी में स्थित है। भारतीय संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन है जबकि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है । ये दोनों सदन भारत की संसद के कामकाज को सुचारू बनाते हैं। इस लेख में, हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी, उनके कार्य और लोकसभा और राज्यसभा के बीच तुलना के बारे में बताते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर
भारत में संसद के रूप में द्विसदनीय विधानमंडल है । भारतीय राजनीति में ‘लोकसभा’ और ‘राज्यसभा’ का नामकरण 1954 में अपनाया गया था । भारतीय संसद के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक के हैं । दोनों संसदीय सदन कई पहलुओं में एक दूसरे से भिन्न हैं।
| तुलना का आधार | लोकसभा | राज्य सभा |
| परिभाषा | इसे निचले सदन या जनता के सदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां भारत के बेहतर शासन के लिए विधेयक पारित किए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं। | इसे संसद या राज्य परिषद के ऊपरी सदन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न राज्यों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। |
| संवैधानिक प्रावधान | अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना से संबंधित है। | अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना से संबंधित है। |
| कार्यकाल अवधि | लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। | राज्यसभा के लिए कोई कार्यकाल अवधि नहीं है क्योंकि यह संसद का एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन हर 2 साल के बाद, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। |
| सदस्यता के लिए चुनाव | लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता की भागीदारी से मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। | राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। |
| चुनाव सिद्धांत | सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा चुनाव के लिए लागू किया जाता है। | राज्य सभा चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू किया जाता है। |
| ताकत | लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से 552 तक होती है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। | राज्य सभा की सदस्य संख्या 200 से 250 तक होती है। वर्तमान में राज्य सभा में 245 सीटें हैं। |
| न्यूनतम आयु | लोकसभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। | राज्य सभा का सांसद बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। |
| सदन प्रतिनिधि | लोक सभा का कार्य लोक सभा अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है। | राज्य सभा का कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सभापति के रूप में संचालित किया जाता है। |
| भूमिका | राज्य सभा की तुलना में कानून बनाने और धन विधेयक पारित करने में लोक सभा की भूमिका अधिक है। | राज्य सभा को राज्य सूचियों पर कानून बनाने और नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का विशेष अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। |
लोक सभा और उसके कार्य
भारतीय राजनीति के अध्ययन में लोकसभा को लोगों का सदन माना जाता है । यह यहाँ विधेयकों को पारित करके भारत में कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2019 में भारत में सत्रहवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ। लोकसभा का आम चुनाव हर पाँच साल में होता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार अपने कार्यों को पारदर्शी तरीके से करे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि वित्तीय मामलों को तय करने में लोकसभा की भूमिका अधिक होती है ।
लोक सभा के कार्य
लोक सभा के पास कई कार्य हैं जैसे कानून बनाना, राष्ट्रीय हित के विषयों पर चर्चा करना, वित्तीय प्रशासन के लिए धन विधेयक पारित करना, तथा सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए अपना अध्यक्ष चुनना।
1. विधानमंडल
लोकसभा को सदन से विधेयक पारित करके देश के नए कानून बनाने का अधिकार है। इस कानून में मौजूदा कानूनों में संशोधन और निरसन भी शामिल है । असाधारण परिस्थितियों जैसे आपातकालीन मामलों में, यदि कोई विधेयक संसदीय सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो वह विधेयक कानून बन जाता है और एक वर्ष के लिए वैध रहता है। यदि संसदीय सदनों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है । संसद की संयुक्त बैठक में, लोकसभा का अध्यक्ष संसद की अध्यक्षता करता है और कानून बनाने के मामले में लोकसभा, राज्यसभा से अधिक सशक्त होती है।
2. वित्तीय मामले
धन विधेयक हमेशा लोकसभा के सदस्यों द्वारा शुरू किए जाते हैं । लगभग सभी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा समान रूप से पारित किए जा सकते हैं, लेकिन केवल धन विधेयक के मामले में, लोकसभा राज्यसभा पर हावी होती है। यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा बनाया और पारित किया जाता है, तो उसे राज्यसभा की सहमति और सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा से लोकसभा को सुझाव भेजने के लिए न्यूनतम समय अंतराल 14 दिन है। राज्यसभा के दिए गए सुझावों से लोकसभा के लिए सहमत होना कोई अनिवार्यता नहीं है।
3. चुनाव और संरचना
अनुच्छेद 81 भारतीय संविधान इसमें कहा गया है कि लोक सभा में भारत के राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और संघ शासित प्रदेशों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे । लोक सभा अपना अध्यक्ष भी चुनती है जो सदन में कामकाज का संचालन करता है।
4. सार्वजनिक शक्तियां
लोकसभा के सदस्य आम तौर पर निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बहस और चर्चा करने का अधिकार होता है । संसदीय सदन की चर्चाएँ वित्तीय मामलों, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकती हैं। संसदीय चर्चाएँ और बहसें भारतीय राजनीति में जाँच और संतुलन का काम करती हैं ।
राज्य सभा और उसके कार्य
भारतीय राजनीति के अध्ययन में राज्य सभा को राज्यों की परिषद माना जाता है। भारत में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय विधानमंडल के प्रति भारतीय राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। राज्य सभा संसद का स्थायी सदन है और इसे किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के आम चुनाव के विपरीत, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है । हर दूसरे वर्ष, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं ।
राज्य सभा के कार्य
- राज्य सभा संसद के सदन के रूप में कार्य करती है जो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है ।
- किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है ।
- राज्य सभा को लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करके तथा उन पर सुझाव देकर लोक सभा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कई राज्यों की विधान सभा/विधानसभा के प्रतिनिधियों या निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने का विशेष अधिकार राज्य सभा को है । इसके लिए प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना होता है ।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार राज्य सभा को है । इसके लिए प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से समर्थन मिलना चाहिए ।
लोक सभा और राज्य सभा के विविध कार्य
- भारतीय संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जाता है ।
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है ।
- राज्यसभा की कार्रवाई के मामले में, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने जैसे हर मामले में लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है ।
इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में कई विषयों पर विधेयक पारित करने की निर्णायक शक्ति है । राज्यसभा भारतीय संसद की द्विसदनीय व्यवस्था को बनाए रखती है जबकि लोकसभा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है।