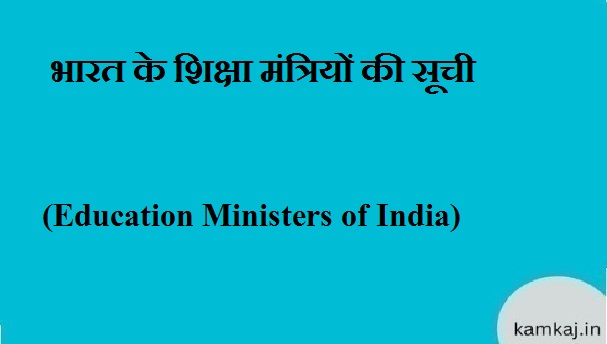स्वतंत्रता के बाद से साक्षरता दर 12% से बढ़कर वर्तमान वर्षों में 75% हो गई है। भारत में, स्वतंत्रता के समय से शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है और यह परिवर्तन हमारे नेताओं की महान निष्ठा और समर्पण के कारण है, जिन्होंने शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की। अब तक 30 से अधिक शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। इन सभी ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में सराहनीय कार्य किए हैं।
भारत के शिक्षा मंत्रियों की सूची
भारत के शिक्षा मंत्रियों ने भारत में शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के समय 12% साक्षरता दर से लेकर वर्तमान युग में 75% साक्षरता दर तक हमारे महान नेता की महान भूमिका रही है। हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश को शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में शिक्षा प्रणाली में नए सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन चल रहा है। नीचे भारत के शिक्षा मंत्रियों की सूची उनके कार्यकाल सहित दी गई है:
| क्र.सं. | भारत के शिक्षा मंत्री | कार्यालय की अवधि |
| 1. | मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद | 15 अगस्त 1947 – 22 जनवरी 1958 |
| 2. | डॉ. केएल श्रीमाली | 22 जनवरी 1958 – 31 अगस्त 1963 |
| 3. | श्री हुमायूं कबीर | 1 सितम्बर 1963- 21 नवम्बर 1963 |
| 4. | श्री एम.सी. छागला | 21 नवम्बर 1963- 13 नवम्बर 1966 |
| 5. | श्री फखरुद्दीन अली अहमद | 14 नवम्बर 1966- 13 मार्च 1967 |
| 6. | डॉ. त्रिगुणा सेन | 16 मार्च 1967- 14 फ़रवरी 1969 |
| 7. | डॉ. वीकेआरवी राव | 14 फ़रवरी 1969 – 18 मार्च 1971 |
| 8. | श्री सिद्धार्थ शंकर रे | 18 मार्च 1971 – 20 मार्च 1972 |
| 9. | प्रो. एस. नूरुल हसन | 24 मार्च 1972- 24 मार्च 1977 |
| 10. | प्रो. प्रताप चंद्र चंद्र | 26 मार्च 1977 – 28 जुलाई 1979 |
| 11। | डॉ. करण सिंह | 29 जुलाई 1979 – जनवरी 1980 |
| 12. | श्री बी. शंकर आनंद | 14 जनवरी 1980- 18 अक्टूबर 1980 |
| 13. | श्री एस.बी.चव्हाण | 17 अक्टूबर 1980- 8 अगस्त 1981 |
| 14. | श्रीमती शीला कौल | 10 अगस्त 1981- 31 दिसम्बर 1984 |
| 15. | श्री के.सी. पंत | 31 दिसंबर 1984- 25 सितंबर 1985 |
| 16. | श्री पी.वी. नरसिम्हा राव | 25 सितम्बर 1985- 25 जून 1988 |
| 17. | श्री पी. शिवशंकर | 25 जून 1988- 2 दिसंबर 1989 |
| 18. | श्री वी.पी.सिंह | 2 दिसंबर 1989- 10 नवंबर 1990 |
| 19. | श्री राज मंगल पांडे | 21 नवम्बर 1990- 21 जून 1991 |
| 20. | श्री अर्जुन सिंह | 23 जून 1991 – 24 दिसम्बर 1994 |
| 21. | पी.वी. नरसिम्हा राव (दो बार दोहराया गया) | 25 दिसंबर 1994- 9 फरवरी 1995 |
| 22. | श्री. माधव राव सिंधिया | 10 फरवरी 1995- 17 जनवरी 1996 |
| 23. | पी.वी. नरसिम्हा राव (तीन बार दोहराया गया) | 17 जनवरी 1996- 16 मई 1996 |
| 24. | श्री अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996- 1 जून 1996 |
| 25. | श्री एस.आर.बोम्मई | 5 जून 1996- 19 मार्च 1998 |
| 26. | डॉ. मुरली मनोहर जोशी | 19 मार्च 1998- 22 मई 2009 |
| 27. | अर्जुन सिंह (दो बार दोहराया गया) | 22 मई 2004 – 22 मई 2009 |
| 28. | श्री कपिल सिब्बल | 29 मई 2009- 29 अक्टूबर 2012 |
| 29. | श्री एम.एम.पल्लम राजू | 30 अक्टूबर 2012- 26 मई 2014 |
| 30. | श्रीमती स्मृति ईरानी | 26 मई 2014 – 5 जुलाई 2016 |
| 31. | श्री प्रकाश जावड़ेकर | 5 जुलाई 2016 – 30 मई 2019 |
| 32. | रमेश पोखरियाल | 30 मई 2019- 7 जुलाई 2021 |
| 33. | धर्मेंद्र प्रधान | 7 जुलाई 2021 – वर्तमान |
भारत के शिक्षा मंत्री
इस मिशन को हासिल करने या बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बनाया गया था। भारत में 1947 से शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में, राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) में बदल दिया, और बाद में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नई मसौदा “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” की सार्वजनिक घोषणा के साथ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वर्तमान में, इसके दो विभाग हैं:
- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
जहां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक की देखभाल करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग- यह विभाग भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है।
- उच्च शिक्षा विभाग- यह विभाग माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सलाह पर इस विभाग को शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार है।
शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य
मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य होंगे:
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इसका क्रियान्वयन अक्षरशः हो
- नियोजित विकास में पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों की पहुंच का विस्तार करना तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां लोगों की शिक्षा तक आसान पहुंच नहीं है।
- गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना
- समाज के वंचित वर्गों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- देश में शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनेस्को और विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने सहित शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
भारतीय शिक्षा प्रणाली लंबे समय से दुर्गमता और निम्न-गुणवत्ता वाली शिक्षा की समस्या का सामना कर रही है, जो भारतीयों को बेरोजगार बनाती है। इसके कारण, भारत अपनी मानव पूंजी की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जो किसी राष्ट्र को विकसित करने में मदद करता है और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने भारत में अच्छी शिक्षा प्रणाली को विनियमित करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि वे ही हैं जो आबादी की जरूरतों के अनुसार योजना बनाते हैं और उनसे निपटते हैं और जरूरत के हिसाब से समाधान प्रदान करते हैं।